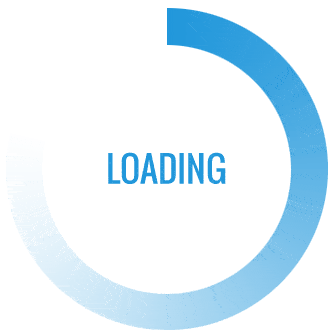हिंदुस्तान का दिल मध्यप्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय उद्यान, प्राकृतिक परिवेश और ऐतिहासिक इमारतों की वजह से तो जाना ही जाता है साथ ही इस सांस्कृतिक विरासत का एक पहलू है, यहाँ का विशिष्ट हथकरघा या हैंडलूम वस्त्र यहाँ की चंदेरी साड़ी पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखती है और हर महिला की पहली पसंद बनी हुई है । रेशम और कॉटन के संयोजन से बनी यह साड़ी ऐसी झिलमिल आभा प्रदर्शित करती है कि इसे हम ”साड़ियों की रानी” भी कह सकते है । इस साड़ी का नाम इसके जनक शहर चंदेरी के नाम पर पड़ा जो मध्यप्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। यह बेतवा नदी के पास विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक छोटा सा शहर है पर इसका अपना एक समृद्धशाली ऐतिहासिक अतीत है, न केवल साड़ी बल्कि अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए भी यह जाना जाता है । भारतीय साड़ी विश्व का पुराना परिधान है, इसी क्रम में चंदेरी साड़ी का भी एक विस्तृत इतिहास रहा है। जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत काल में मिलता है । माना जाता है कि भगवान श्रीकृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल ने इसे रचा था। महाभारत में उल्लेखित मोती कढ़ाई वाली साड़ी चंदेरी साड़ी का संकेत करती है । चंदेरी की बुनाई का तरीका दूसरी से सातवी शताब्दी का है । अन्य लिखित प्रमाण 11वीं शताब्दी से मिलते है। 13वीं और 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग भी उल्लेखित मिलता है कि सूफी संत हजरत वजीउद्दीन बंगाल के लखनोती क्षेत्र से चंदेरी आये, तब उनके बहुत से अनुयायी भी उनके साथ चंदेरी चले आये। तब बंगाल विशेष रूप से ढाका महीन, मलमल के कपड़े की बुनाई के लिए जाना जाता था। बंगाल से चंदेरी आये लोगों ने महीन कपड़े की बुनाई और उत्पादन शुरू किया | ये सब मुस्लिम समुदाय से सम्बंधित थे, बाद में झाँसी के कोष्टी बुनकर भी 1350 के दशक में चंदेरी में आकर बस गए और चंदेरी बुनाई को उन्नत किया । चूँकि चंदेरी आये मजदूर बुनकर भी उसी क्षेत्र से सम्बंधित थे तो मलमल निर्माण प्रक्रिया भी ढाका के समान रही और ढाका के मलमल के साथ चंदेरी मलमल भी प्रसिद्ध हुआ । ढाका और चंदेरी के मलमल में साम्य की वजह से नगर में एक कहावत प्रचलित रही-: “ढाका और चंदेरी में मलमल महीन बनती थी । पूरे भारत में चंदेरी की पहली गिनती थी |”

चंदेरी हस्तशिल्प कला का जन्म मलमल कपड़े के रूप में हुआ। बाद में इससे राज परिवारों के लिए वस्त्र बनाये जाने लगे। तब राजघरानों के लिए परिधान साड़ी, पगडा, दुपट्टा ,शॉल ,ओढ़नी, पर्दा आदि बनाए जाते थे । 15वीं शताब्दी में मालवा के सुल्तानों द्वारा भी इसे संरक्षण दिया गया । मुगल साम्राज्य के समय चंदेरी का यह हस्तशिल्प सबसे ज्यादा बढ़ कर अपने चरम पर पहुंचा। मुगलकाल में इन साड़ियों को बनाने के लिए ढाका से बारीक मलमल के रेशे मंगवाए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि यह साड़ी इतनी बारीक होती थी कि पूरी साड़ी एक मुट्ठी में समा जाती थी । इससे जुड़ा एक मशहूर प्रसंग है कि मुगल बादशाह अकबर को चंदेरी का बना वस्त्र एक छोटे से बांस के खोल में बंद करके भेजा गया था । जब चंदेरी कपड़े को बांस के खोल से बाहर निकाला गया तो उससे एक पूरा हाथी ही ढक गया। सोने के जरदोजी काम की वजह से चंदेरी साड़ियां और भी अधिक प्रसिद्ध हुई । इन पर मोहक मीनाकारी व अड्डेदार पटेला का काम भी किया जाता था।वस्त्रों में रेशम कतान सूत, मर्सराइज्ड विभिन्न रंगों की जरी और चमकीले तारों का प्रयोग किया जाता था। धागों की कताई-बुनाई, रंगाई आदि कार्य बुनकर स्वयं करते थे । ऐसा कहा जाता है कि बड़ौदा की महारानी बुनकरों को खुद बेहतरीन सूत देकर उनसे साड़ियां बनवाया करती थी । वह कपड़े की परख उसे अपने गालों पर रगड़कर किया करती थी, इससे वस्त्र की महीनता और क्वालिटी का पता लग जाता था। तब मराठा शासकों के लिए भी विशेष रूप से चंदेरी वस्त्र बनाए जाते थे । राजपरिवारों के लिए पगड़ी, साफे, धोती आदि ही मुख्यत: प्रचलन में थे, फिर के साड़ी के रूप में भी धीरे-धीरे चंदेरी प्रसिद्ध हुआ । पहले यह साड़ी केवल राजघरानों में ही पहनी जाती थी । तब राज परिवारों की स्त्रियां केसर से निकाले गए रंग में अपनी साड़ियों के धागे रंगवाती थी, जिन्हें पहनने के बाद केसर की भीनी खुशबू आती थी । चंदेरी वस्त्र बारीक, पारदर्शी, वजन में हल्के, कशीदाकारी आदि के कारण भारत के विभिन्न भागों में राज कर रहे राजवंशों द्वारा पसंद किए गए । तब चंदेरी महत्वपूर्ण सैनिक केंद्र था और प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी यही से होकर गुजरते थे। मालवा एवं बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण यह नगर एक व्यापारिक केंद्र बनकर उभरा जिसका संपूर्ण व्यापार हथकरघा व चंदेरी वस्त्र आधारित था । 15-16 वीं सदी में भी चंदेरी अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण सामाजिक, राजनीतिक तथा व्यापारिक महत्व बनाए हुए था। चंदेरी गागरोन राजा मेदिनी राय राजपूत के समय राजस्थान से मारवाड़ी परिवारो का चंदेरी आगमन और साड़ी व्यापार से जुड़ना चंदेरी हथकरघा के लिए बहुत लाभदायक हुआ । मुगल काल में चंदेरी नगर में राजकीय संरक्षण प्राप्त शाही कारखाना स्थापित किया गया ताकि कपड़ा उत्पादन बेहतरीन बनाया जा सके । 17वीं और 18वीं सदी में चंदेरी पर बुंदेल राजाओं का शासन रहा तब भी यह कला विकास के नए सोपान पर चढ़ती रही और चंदेरी निर्मित सूती कपड़ा निर्यात किया जाने लगा। उनके शासनकाल में पारंपरिक चंदेरी कपड़ों की गुणवत्ता की परख उस पर लगी शाही मुहर,जिसमें ताज और ताज के दोनों ओर खड़े शेर अंकित होते थे,से की जाती थी । कालांतर में चंदेरी वस्त्रों पर बादल महल दरवाजे की मुहर लगाई जाने लगी ।

17वीं सदी में चंदेरी साड़ियां बनने के लिए मैनचेस्टर से सूती धागा मंगाया जाने लगा, जो कोलकाता बंदरगाह से होते हुए चंदेरी तक पहुंचता था। उसके बाद साड़ियां बुनने के लिए जापान, चीन और कोरिया से भी रेशम मंगाया जाने लगा और चंदेरी साड़ियां सिल्क से भी बुनी जाने लगी।जब 300 काउंट वाले सूती कपड़े का ईजाद हुआ तब यह कपड़ा आंध्रप्रदेश के कोलीकंडा के पेड़ की जड़ से तैयार बेहतरीन धागों से बुना जाने लगा। इससे चंदेरी साड़ियां बंगाल के मलमल से टक्कर लेने लगी । सन 1890 में जब बुनकरों के हाथों से निर्मित यार्न के स्थान पर मिल द्वारा निर्मित यार्न से कपड़ा बुना जाने लगा तब चंदेरी के विकास ने भी गति पकड़ी। चंदेरी फैब्रिक के निर्माण के लिए मिलमेड यार्न के उपयोग के बाद अंग्रेज मैनचेस्टर से कोलकाता होते हुए सूती धागा चंदेरी लेकर आएं। यह चंदेरी फैब्रिक के इतिहास में एक बड़ा बदलाव हुआ। 19वीं सदी में जब चंदेरी ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आई तो सिंधिया घराने ने भी इस हस्तकला को संरक्षण दिया। वर्ष 1910 में तत्कालीन सिंधिया परिवार ने नगर में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की तथा इस शिल्पकला के संरक्षण व संवर्धन के प्रयास किए। वर्तमान में भी उसी प्रशिक्षण केंद्र में ही शासकीय प्रशिक्षण केंद्र और साड़ी संग्रहालय शासन द्वारा संचालित है । वर्ष 1930 में जब कपड़े के वार्प अर्थात ताने में जापानी सिल्क और वेफ्ट अर्थात बाने में कॉटन का प्रयोग हुआ तब इससे चंदेरी फैब्रिक की मजबूती कम हुई, दोनों प्रकार के धागे सही प्रकार से नहीं जुड़ने के कारण फैब्रिक मुड़ जाते थे और साड़ी तह वाली जगहों से फट जाती थी । वर्ष 1970 के लगभग बुनकरों ने इसके विपरीत काटन के ताने और सिल्क के बाने का प्रयोग किया तब इससे चंदेरी कपड़ा पहले की अपेक्षा अधिक मजबूत हुआ है। पहले केवल राजघरानों द्वारा पहने जाने वाली चंदेरी वस्त्र व साड़ी एक लंबी यात्रा करके अब आम जन तक भी पहुंच गए हैं । इम्पेरियर गजेटियर ऑफ इंडिया में चंदेरी बुनाई का उल्लेख है, इसमें लिखा है “चंदेरी लंबे समय से नाजुक मलमल कपड़े के लिए
प्रसिद्ध है ।” देश की आजादी के बाद 1 नवंबर 1956 को मध्यप्रदेश राज्य गठन के साथ ही शासन के संरक्षण में इस उद्योग के संवर्धन हेतु व्यापक प्रयास तथा इंतजाम किए गए हैं । चंदेरी साड़ी बनाने की प्रक्रिया के चरण भी जटिल हैं । चंदेरी साड़ी बनाने के लिए बुनकर सबसे पहले ताना के धागों की रंगाई का कार्य करते हैं इसके उपरांत ताना भरा जाता है, जिसे बीम भरना कहते हैं । इसके लिए लंबे स्थान तथा दो बुनकरों की जरूरत होती है। इसके बाद ताना जुड़ाई , नाका बांधना आदि कार्य किए जाते हैं । ठीक इसी प्रकार बाना में उपयोग किए जाने वाले धागा कतान आदि रंगाई उपरांत बाबीन भरना प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसे चरखानुमा उपकरण चलाकर पूर्ण करते हैं जिसे विमल भरना कहा जाता है । बुनाई शुरू करने के लिए सबसे पहले साड़ी की बूटी ,बॉर्डर और किनारी के अनुपात में अलग-अलग रंगों के धागे करघे पर चढ़ा दिए जाते हैं । इसके बाद धागा हथकरघा ताना-बाना में फिट करके साडी की बुनाई की जाती है । बुनाई के साथ ही छोटी-बड़ी बूटी ऑर्डर व डिजाइन बनाई जाती है । अंत में खूबसूरत पल्लू की बुनाई की जाती है । इस प्रकार तैयार होती है एक अद्भुत अद्वितीय चंदेरी साड़ी । चूंकि साड़ी बनने की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है । सूती-रेशमी धागों का उचित संयोजन, उचित रंग तथा बॉर्डर का समायोजन आदि काफी श्रमसाध्य व समयसाध्य है, इसीलिए एक बार में ही बारह साड़ियों का कच्चा मटेरियल तैयार कर लिया जाता है ।

साड़ी के लिए आवश्यक रेशम, सूती धागा,कतान तथा जरी देश के अलग-अलग भागों से व्यापारी उपलब्ध करा देते हैं। पहले साड़ी में मात्र असली जरी( सोना चांदी युक्त) का उपयोग होता था। वर्तमान में इसकी जरी में चांदी से बने धागों में सोने का पानी चढ़ा हुआ होता है। यह जरी आगरा और सूरत से मंगाई जाती है । वाराणसी की जरी भी चंदेरी साड़ियों के लिए अच्छी मानी जाती है । जरी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर है कि उसमें कितनी मात्रा में असली चांदी है। असली चांदी की जरी के इस्तेमाल से साड़ी की लागत और कीमत बढ़ जाती है, इसलिए अधिकतर बुनकर जरी के कृत्रिम धागों में थोड़ी सी चांदी मिलाकर साड़ी की किनारी तैयार कर लेते है । पूर्व में दो बुनकरों द्वारा हाथ से चलने वाली हस्तचलित थ्रोशटल पद्धति वाले नाल फेरमा करघे का स्थान उन फ्लाई शटल वाले लूम ने ले लिया है जिससे एक ही बुनकर अपने हाथ व पैरों से करघे को संचालित करता है, और अकेला बुनकर भी काम करने में सक्षम हो गया है । साथ ही नई प्रणाली में जैकार्ड और डॉबी के उपयोग से साड़ी के बॉर्डर भी आसनी से बनाए जाने लगे है। पहले चंदेरी साड़ियां केवल सफेद सूत से तैयार की जाती थी। धीरे-धीरे सफेद रंग पर बॉर्डर तथा प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर कपड़े रंगे जाने लगे। प्रारंभ में फूलों,केसर आदि से प्राप्त रंग प्रयुक्त होते थे अब पक्के रसायनिक रंग इस्तेमाल किए जाने लगे हैं ।
चंदेरी साड़ियों के पृष्ठभूमि तथा बॉर्डर का विरोधी रंग संयोजन किया जाता है । जैसे काले के साथ लाल बॉर्डर साड़ियों में सामान्यतः नारंगी,लाल, गुलाबी,बादामी, तोतापंखी, केसरिया आदि रंगों का इस्तेमाल होता है । हल्के तथा गहरे रंग के संयोजन से साड़ी अपने आकर्षक हो जाती है । हल्के गहरे रंग के संयोजन वाली इन साड़ियों को गंगा जमुना साड़ी कहते हैं। चंदेरी साड़ी के कोमल रंग रेशमी चमक और सोने की जरी के बॉर्डर तथा बुरी इसकी विशिष्टता में वृद्धि करते है । चंदेरी की बुनाई सधे हुए हाथों से बारीकी के साथ की जाती है । एक चंदेरी साड़ी बनाने में कई दिनों बल्कि कई बार कई महीनों का समय लगता है । इसीलिए चंदेरी साड़ियों को बनाते समय कारीगर इसे बाहरी नजरों से बचाने के लिए हर मीटर पर काजल का टीका लगाते हैं । हथकरघा पर बनी विशेष पारंपारिक साड़ियों के जैसी अनूठी डिजाइन दूसरी नहीं मिलती। बारीक जरी की बॉर्डर चंदेरी साड़ियों की खास पहचान है। सदियों से चली आ रही चंदेरी साड़ियां सदियों से अपनी पारदर्शी बारीक बुनाई और साड़ियों में बनाई जा रही बूटियों के कारण प्रसिद्ध है । नजाकत, महीनता और पारदर्शी झिलमिलापन साड़ी का यह महत्वपूर्ण व अद्वितीय गुण है जो सामान्यतः किसी अन्य कपड़ों में देखने नहीं मिलता । चंदेरी साड़ियों के प्रसिद्ध पैटर्न नलफर्मा, डंडीदार, चटाई, फूल-पत्ती, दो-चश्मी, अखरोट, पान, सर्रजबूटी, कमली, जंगला और मेहंदी वाले हाथ आदि प्रसिद्ध है । इसके अलावा गोल्डन सिक्के, चूड़ी,बूंदी घुंघरू, डंडीदार, चटाई, भी प्रचलित है । कई पैटर्न मुगल कला से प्रभावित है । चंदेरी बॉर्डर में भी नक्शी,जरी पटले पाईपिंग आदि प्रचलित पैटर्न है।अब बदलते परिवेश में साँची के स्तूप खजुराहो के मंदिर की नृत्यांगनाओं के चित्र, बारात संग दुल्हन की डोली का दृश्य जैसे अद्वितीय चित्रण भी चंदेरी पर हो रहा है ।